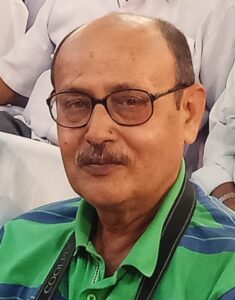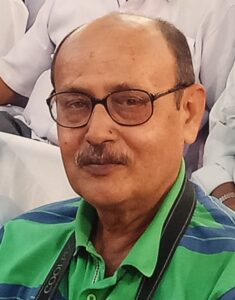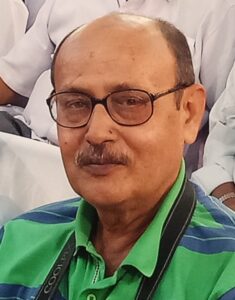शरद बिल्लौरे की कविताएँ

प्रस्तुति : सरिता सिंह
भाषा
“”””””””
पृथ्वी के अंदर के सार में से
फूट कर निकलती हुई
एक भाषा है बीज के अँकुराने की।
तिनके बटोर-बटोर कर
टहनियों के बीच
घोंसला बुने जाने की भी एक भाषा है।
तुम्हारे पास और भी बहुत-सी भाषाएँ हैं,
अण्डे सेने की
आकाश में उड़ जाने की
खेत से चोंच भर लाने की।
तुम्हारे पास
कोख में कविता को गरमाने की भाषा भी है
तुम बीज की भाषा बोलीं
मैं उग आया
तुमने घोंसले की भाषा में कुछ कहा
और मैं वृक्ष हो गया।
तुम अण्डे सेने की भाषा में गुनगुनाती रहीं
और मैं आकार ग्रहण करता रहा।
तुम्हारे आकाश में उड़ते ही
मैं खेत हो गया।
तुमने चोंच भरी होने का गीत गाया
और मैं नन्हीं चोंच खोले
घोंसले में चिंचियाने लगा।
तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं
तुम्हारी कोख में गरमाती
कविता में भाषा बोल रहा हूँ।
**”””””“””“”“””“
ये पहाड. वसीयत हैं
“””””””””””””””””””””””””””””
ये पहाड़ वसीयत हैं
हम आदिवासियों के नाम
हज़ार बार
हमारे पुरखों ने लिखी है
हमारी सम्पन्नता की आदिम गंध हैं ये पहाड़।
आकाश और धरती के बीच हुए समझौते पर
हरी स्याही से किए हुए हस्ताक्षर हैं
बुरे दिनों में धरती के काम आ सकें
बूढ़े समय की ऎसी दौलत हैं ये पहाड़।
ये पहाड़ उस शाश्वत गीत की लाइनें हैं
जिसे रात काटने के लिए नदियाँ लगातार गाती हैं।
हरे ऊन का स्वेटर
जिसे पहन कर हमारे बच्चे
कड़कती ठण्ड में भी
आख़िरकार बड़े होते ही हैं।
एक ऎसा बूढ़ा जिसके पास अनगिनत किस्से हैं।
संसार के काले खेत में
धान का एक पौधा।
एक चिड़िया
अपने प्रसव काल में।
एक पूरे मौसम की बरसात हैं ये पहाड़।
एक देवदूत
जो धरती के गर्भ से निकला है।
दुनिया भर के पत्थर-हृदय लोगों के लिए
हज़ार भाषाओं में लिखी प्यार की इबारत है।
पहाड़ हमारा पिता है
अपने बच्चों को बेहद प्यार करता हुआ।
तुम्हें पता है
बादल इसकी गोद में अपना रोना रोते हैं।
परियाँ आती हैं स्वर्ग से त्रस्त
और यहाँ आकर उन्हें राहत मिलती है।
हम घुमावदार सड़कों से
उनका शृंगार करेंगे
और उनके गर्भ से
किंवदन्तियों की तरह खनिज फूट निकलेगा।
“”””‘“””“”””‘“”””**
तब एक कविता लिखी गई होगी
“”””'””””‘””‘””””””””””””””””””'””””””‘””””””””””””
तब
रात्रि के देवता ने करवट ली होगी
और आसमान में
एक साथ हिनहिनाए होंगे
चाँदी के घोड़े
तब
एक बैल शरीर झटक कर खड़ा हो गया होगा
और एक ने
सिर्फ़ हवा को सूँघ कर ही
गरदन नीची कर दी होगी
तब एक चूल्हा धुंधुआया होगा
और एक लकड़ी
मुँह बिदकाए बिना गुटक गई होगी
लोहे का कसैला स्वाद
तब
एक बीज ज़मीन के भीतर तक गया होगा
और एक सपना अँकुराया होगा
नींद से एकदम बाहर
तब एक आदमी ने आकाश की तरफ़ देखा होगा
और एक औरत
धरती में छुपा आई होगी
अपने बालों का मैल
तब
एक कविता लिखी गई होगी
एक कौआ उड़ा होगा
और एक गाय की पीली दाढ़ में
भर गया होगा
नरम घास का रस।
“”””‘“”””’“””””*””””
साईकिल
“””””””””””””””””
ठीक अपने मालिक की तरह
उसकी उम्र की गिनती भी
पैदा होने के दिन से नहीं
काम पर आने के दिन से होती है।
बूढ़े के साथ बूढ़ी
और
जवान के साथ जवान
साइकिल की नींद में हैं
तीन चीज़
सड़क
पैर
हवा।
सड़क की नींद में जूते
पैर की नींद में घास
हवा की नींद में पत्तियाँ
साइकिल किसी की नींद में नहीं।
जैसी कि
हमारे घर में अकेली साइकिल
और साइकिल के घर में
हम-सब।
अम्मा, बुआ और भाई-बहन
कुल मिलाकर नौ
एक साथ सबको ख़ुश नहीं कर पाती।
सिर्फ़ घण्टी बजने जितनी मोहलत मांगने
महराबदार रास्तों में
बार-बार भटकी
इतनी-इतनी चढ़ाइयाँ
कि सड़क ढली
हवा रुकी
पैर थके
साइकिल नहीं थकी।
जब तक वह घर में है
बापू की यादगार है।
“””‘“”‘”“”””“”‘”‘“
बैल
“””””””””’
पूरे दिन
अपने-अपने भविष्य को कंधा देने के बाद
शाम आने पर
बैल अकसर जुगाली करते हैं
और आदमी बातें।
कभी-कभी बैल बतियाते हैं
एक-दूसरे से
कि आदमी काम करते वक़्त
मुड़-मुड़ कर देखता क्यों है?
दूसरा कहता है
अपनी नाक में रस्सी नहीं होती
तो अपन भी मुड़कर नहीं दॆकते क्या?
आदमी की नाक में कौन-सी रस्सी है
कौन खींचता है उसे?
बैल जब-जब यह बात
आदमी से पूछते हैं
आदमी जुगाली करता हैं
“””””“””“”””“””**
मुझे उगने तो दो
“”””””””””””””””””””””””””””
आख़िर कब तक तलाशता रहूंगा
सम्भावनाएँ अँकुराने की
और आख़िर कब तक
मेरी पृथ्वी
तुम अपना गीलापन दफ़नाती रहोगी,
कब तक करती रहोगी
गेहूँ के दानों का इन्तज़ार
मैं जंगली घास ही सही
तुम्हारे गीलेपन को
सबसे पहले मैंने ही तो छुआ है
क्या मेरी जड़ों की कुलबुलाहट
तुमने अपने अंतर में महसूस नहीं की है
मुझे उगाओ मेरी पृथ्वी
मैं उगकर
कोने-कोने में फ़ैल जाना चाहता हूँ
तुम मुझे उगने तो दो
मैं
तुम्हारे गेहूँ के दानों के लिए
शायद एक बहुत अच्छी
खाद साबित हो सकूँ
“””’‘”””“”**””””“””
रात
“””””””
कन्धे पर टँगे थैले से लेकर
बिस्तर तक
कितना कुछ हो गया होता है
रात देर गये
जब हम अपने घरों में लौटते हैं।
कितना भारी-भारी हो गया होता है हमारा घर
तलुओं और पिण्डलियों के भीतर
फड़फड़ाती थकान
और पोर-पोर से फूटता दर्द
हमारे ठण्डे खाने को कितना गर्म कर देता है।
हमारे शरीर की चुप्पी
शहर पर कितनी जल्दी छा जाती है
और कितनी नींद में होती हैं हमारी चेतना
कि जब हमारी मेडिकल रिपोर्टों में
कुछ भी नार्मल नहीं होता
तो किसी को भी आश्चर्य नहीं होता।
हमारे भीतर पनप रहे
किसी गम्भीर रोग की चिन्ता में
सिर्फ़ हमारी प्रेमिकाएँ कुछ देर सुबकती हैं
और सम्बन्ध तोड़ लेती हैं,
घर की चिट्ठी
राशन कार्ड
और लकड़ी के सपनों को ओढ़कर।
जब हम
अपनी फटी पैंट को पलटवाने के बारे में
सोचते हुए
अचानक सो जाते हैं।
हमारे भीतर पल रहे रोग का चेहरा
उतर जाता है
और हमारे शहर में
एक सड़क
हम लोगों को याद करती हुई
रात भर जागती है।
“”””””””””””””””””””””””””‘”””””””””””
कविता-संग्रह
तय तो यही हुआ था
जन्म: 19 अक्तूबर 1955
निधन: 3 मई 1980
जन्म स्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत
कुछ प्रमुख कृतियाँ
तय तो यही हुआ था (1982), अमरू का कुर्ता (नाटक)
विविध
कुल सौ कविताएँ लिखीं। अपनी उन्हीं कविताओं से हिन्दी कविता में अपनी पहचान बना ली।