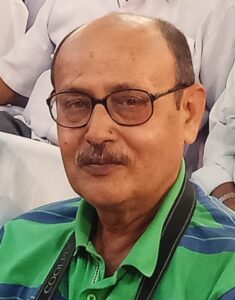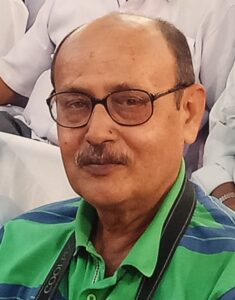सामयिकी @ डॉ. दीपक पाचपोर

चुनाव जीतने लोकतंत्र को दांव लगाते सियासी दल
-डॉ. दीपक पाचपोरलोकतांत्रिक प्रणाली का आधार ही लोगों की सहभागिता है। राज्य एवं सरकार से भी अधिक महत्वपूर्ण ‘नागरिक’ नामक तत्व होता है। अन्य किसी भी तरह की शासन प्रणाली (यथा राजशाही, तानाशाही, सैनिक शासन आदि) में भी ये ही त्रिआयाम बनकर देश बनाते हैं; फिर भी फर्क यह है कि अन्य दोनों में शासक को सत्ता में बिठाने या उसे हटाने का हक जनता के हाथों में नहीं होता। ऐसी कोई प्रक्रिया ही नहीं होती कि शासक के चयन में आमजन भागीदारी निभा सकें। इससे अलग लोकतंत्र के केन्द्र में जनता ही है। उस गण को साधने के लिये अगर राजनैतिक दल कोशिशें करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उल्टे, यह उसके अधिकार में तो है ही, प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा भी है। अगर यह न हो तो जनतांत्रिक व्यवस्था की अपरिहार्य शर्तें पूरी हो ही नहीं सकतीं। भारत के सन्दर्भ में दुखद तो यह है कि जनता को अपने पक्ष में करने के लिये राजनैतिक दल देश एवं समग्र लोकतंत्र को ही खतरे में डाल रहे हैं। इस प्रक्रिया में वे भारतीय संस्कृति एवं दर्शन के खिलाफ होकर भी काम कर रहे हैं।
आजाद भारत के प्रारंभिक दो-तीन दशकों तक तो हमारी विधायिकाओं के चुनाव विकास एवं आर्थिक मुद्दों पर लड़े जाते रहे। मत विभाजन एवं बहस का ज्यादातर आधार विकास के मॉडल को चुनने को लेकर हुआ करता था। दक्षिणपंथी विचारों के दल जहां पूंजीवादी प्रणाली के पक्षधर थे, वहीं समाजवादी एवं साम्यवादी दल संसाधनों व पूंजी के समान बंटवारे के हिमायती थे। इन दोनों ध्रुवों के बीच जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने मध्य मार्ग अपनाया था, बावजूद इसके कि वे यूरोपीय वामपंथ से बेहद प्रभावित थे। अपने कामों के आधार पर वे जनता से वोट मांगते एवं चुनाव जीतते हुए सरकारें चलाते रहे। परवर्ती प्रमं लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस परम्परा को बनाए रखा। इंदिरा गांधी ने भारतीय राजनीति की धारा इस रूप में बदली कि उन्होंने राज्यों की जनसंख्या के सामाजिक गठन के अनुरूप मुख्यमंत्री नियुक्त करने एवं चुनावी पाकेट्स बनाने शुरू किये। हालांकि उनके कार्यकाल में यह तरीका बहुत सघनता से नहीं अपनाया गया। 1998 का लोकसभा चुनाव इस मायने में निर्णायक मोड़ साबित हुआ कि वह ‘मंडल बनाम कमंडल’ की लड़ाई बन गया था। यह एक तरह से ट्रेंड सेटर बन गया जिसके बाद सभी छोटे-बड़े चुनाव तो इस आधार पर लड़े ही जाने लगे, पूरे समाज का इसी आधार पर विभाजन हो गया। तत्कालीन पीएम वीपी सिंह द्वारा मंडल आयोग लागू करने का उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ कमजोर वर्गों के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण था, परन्तु वह सामाजिक विभक्तिकरण का सबब बन गया। इसके साथ ही बाबरी मस्जिद का मसला साम्प्रदायिक विभाजन की बुनियाद भी बन बैठा। उसके बाद तो भारतीय राजनीति की राह ही बदल गयी। मंडल ने अगर देश को अगड़े-पिछड़ों में बांटा तो कमंडल ने हिंदू-मुसलिमों के बीच साम्प्रदायिक विभाजन कराया। ऐसा नहीं कि यह अलगाव पहले भारतीय समाज में नहीं था। था, पर वह ऐसा सघन और गहन नहीं था। ऐसा आक्रामक भी नहीं। ऐसा विस्तृत भी नहीं कि देश की सारी समस्याएं इसके सामने छोटी पड़ जायें और इतना प्रभावशाली भी नहीं कि वही हमारी सारी दिक्कतों का कारण एवं समाधान बन जाये। इसी विभाजनकारी राजनीति की यह यात्रा इतनी आगे निकल आई है कि अब वह ‘80 बनाम 20’ की लड़ाई तक बन गयी है। बहुत पुरानी बातें न की जायें तो चाहे वह नागरिकता कानून हो ( जिसके क्रियान्वयन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला भी आया है), कुमार विश्वास द्वारा लगाया गया आरोप जिसके मुताबिक सिख फॉर जस्टिस के नेताओं से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल के संबंध होना, भारत विभाजन की त्रासदी को याद करने हेतु विभीषिका दिवस मनाना, अमर जवान ज्योति का विलय, चुनाव के पहले लखीमपुर खीरी में अपने वाहन से 8 लोगों को कुचलकर मार देने वाले आशीष मिश्र मोनू को जमानत मिलना या बलात्कार के आरोपी राम रहीम का फरलो पर छूटना हो- सारे ही मामलों का संबंध प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से वर्तमान में जारी विधानसभा के चुनाव हैं और उन्हें येन केन प्रकारेण जीतना ही लक्ष्य है।
5 राज्यों के लिये आधे रास्ते तक पहुंच चुके विधानसभा चुनावों में यह साफ दिख रहा है कि अब चुनाव जीतना और सत्ता पर काबिज होना कहीं अधिक अहम है। देश तथा जनता हमारे सियासी दलों की वरीयता में काफी नीचे हैं। आज लाख प्रयासों के बाद भी भारतीय राजनीति का विमर्श विकास नहीं बल्कि भावनात्मक मुद्दे बनकर रह गये हैं। पिछले करीब तीन दशकों से राजनीति के केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी है, वह हमारे समग्र लोकतंत्र का यही विमर्श सेट कर रही है। कई राज्यों में उसकी सरकारें रही हैं और नब्बे के दशक के आखिर से लेकर 2020 के प्रारम्भिक 3 साल तक उसने केन्द्र की सत्ता चलाई थी। बड़ा बदलाव 2014 से आया जब भाजपा ने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की धुरी सम्भाली। प्रारम्भ में तो उनकी सरकार ने आर्थिक मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम लाये, परन्तु वे तमाम असफल साबित हुए हैं। अब तो स्वयं भाजपा उनका उल्लेख न अपनी प्रचार सभाओं में करती हैं और न ही उसके स्टार प्रचारक अपने भाषणों में करते हैं। यह नाकामी उसे उसकी अपनी उसी पिच पर लौटा ले जाती है जिस पर खेलने की वह उस्ताद है- यानी भावनात्मक मुद्दे- यथा साम्प्रदायिकता, धार्मिकता, जातीय समीकरण, ऊथली देशभक्ति, आक्रामक राष्ट्रवाद आदि। यह संग्राम ऐसा भीषण हो चला है कि ज्यादातर दलों के नेता विरोधी विचारधाराओं, दलों एवं नेताओं के प्रति अत्यंत खूंखार हो चले हैं। गैर लोकतांत्रिक व्यवहार का प्रवर्तन एवं संवर्धन वे लोग कर रहे हैं जिन पर हमारी सामाजिक मर्यादाओं एवं आदर्शों को सहेजने-संवर्धित करने की जिम्मेदारी है- यानी हमारे राजनैतिक दल। हमारी सरकारें एवं मंत्रिपरिषदें सिर्फ कार्यपालिका प्रमुख ही नहीं बल्कि लोकतंत्र एवं सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों की अभिरक्षक भी होती हैं। हमारे नेतागण अगर अराजकता की राह पर चलते हैं या अन्य को प्रेरित करते हैं तो हम अनायास ही एक ऐसा समाज बना डालेंगे जिसमें कोई भी न सुरक्षित रहेगा और न ही व्यक्तिगत या सामूहिक विकास हो पायेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी को ‘दीदी ओ दीदी’ कहकर पुकारना, कांग्रेस की सोनिया गांधी, प्रियंका व राहुल पर व्यक्तिगत हमले, विरोधी दलों को ‘माफिया’ बतलाना, असम के मुख्यमंत्री हेमंता विस्व सर्मा द्वारा किसी से पिता का प्रमाण मांगना, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को मुहावरे की आड़ में ‘कुत्ता’ कहना, उप्र के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ‘श्मशान-कब्रिस्तान’, ‘गर्मी उतारने’ या ‘तमंचा-माफिया’ वाली बातें, पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी द्वारा अरविंद केजरीवाल को ‘बाहरी’ बतलाना या फिर से मोदी की बात करें तो “पंजाब से जान बचाकर लौट आने के लिये वहां के सीएम को धन्यवाद” करना, हारने पर उप्र के राज्य केरल, बंगाल या कश्मीर बन जाने का डर दिखलाना, हिन्दू-मुसलिम, भारत-पाकिस्तान, जिन्ना, देशद्रोह, टुकड़े-टुकड़े गैंग, माफिया, तमंचा जैसी भड़काऊ बातें करना- किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली को विनष्ट करने के लिये तो काफी हैं ही, देश को विभाजित करने और आवाम की दुर्गति करने के लिये पर्याप्त भी हैं। चुनाव जीतने की हड़बड़ी और अति महत्वाकांक्षा देश के समाज के साथ संस्कृति को भी बदलकर रख देगी; और यह बदलाव नकारात्मक ही होगा- लिखकर रख लीजिये!
सामयिकी @ डॉ. दीपक पाचपोर, सम्पर्क- 098930 28383